पूरी स्क्रीन पर पढ़ने के लिये पीडीएफ़ बॉक्स के कोने में बने ![]() चिन्ह का प्रयोग करें
चिन्ह का प्रयोग करें

प्रगतिवादियों के विरुद्ध यह आरोप किया जाता है कि वे साहित्य को केवल प्रचारात्मक बना देना चाहते हैं। श्री इलाचंद्र जोशी तथा उनकी ही तरह साहित्य की समस्याओं पर विचार प्रकट करने वाले अनेक छोटे-बड़े आलोचक केवल इसी बात को लेकर प्रगतिवाद को अपने उचित-अनुचित प्रहारों का निशाना बनाते रहे हैं। उनका खयाल है कि उन्होंने प्रगतिवादियों की ऐसी कच्ची नस पकड़ ली है कि उसे दबाते ही वे उसकी श्वास बंद कर सकते हैं। साहित्य के साथ प्रोपैगैंडा शब्द का प्रयोग करना विशेषकर जबकि साहित्य में ‘अमर कलाकारों’ की भरमार हो और हमारा सारा साहित्य ‘विश्वजनीन’ और ‘शाश्वत’ हो, उनकी दृष्टि में ऐसा जघन्य अपराध है, जिसके लिए पाठक प्रगतिवादियों को कभी क्षमा नहीं कर सकते। यह एक ‘हेरेसी’ है जो कि सच्चे साहित्य की जड़ खोदना चाहती है, अतः अग्राह्य तथा दमनीय है।
प्रोपैगैंडा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हो सकता है, हुआ है, और आज भी होता है। प्रगतिवादियों ने जब कभी भी उसका प्रयोग किया है, तब ऐसे सामान्य अर्थ में कि उससे किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य को प्रोपैगैंडा कहकर उन्होंने उसके उत्कृष्ट भावना प्रधान, कल्पनात्मक और कलात्मक गुणों की अवहेलना नहीं की, न उनका बहिष्कार ही आवश्यक समझा है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मैं साहित्य की इस व्याख्या से सहमत हूं अथवा यह दृष्टिकोण सही है – इसका विवेचन मैं आगे करुंगा। किन्तु जोशीजी और उनकी तरह सोचनेवाले आक्षेपकर्ता, खेद है, प्रगतिवादियों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश न कर उसे ऐसे भद्दे अर्थ पहना देते हैं कि वह निन्दनीय दीख उठता है। मुझे यह स्वीकार करने में जरा भी आपत्ति नहीं कि यदि मुझे इन लोगों के लेखों द्वारा ही प्रगतिवाद के दृष्टिकोण से परिचय मिलता, तो मैं उसे इतना वीभत्स और कुत्सित, प्रगतिविरोधी और असाहित्यिक समझता कि मुझे अनायासही प्रगतिवाद से घृणा हो जाती। मैं समझता कि प्र्रगतिवाद कला और साहित्य की कलात्मकता और साहित्यिकता तथा अन्य सभी उन गुणों को जो इन्हें सजीव, मधुर और सुन्दर बनाते हैं, नष्ट कर उनके स्थानपर नीरस ‘वादों’ की व्याख्या, हड़ताल करने के ऐलान और मजदूर-किसान सभाएं या अन्य पार्टियां संगठित करने के प्रोगैम और प्रदर्शनों में गाने योग्य गीत भरना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को साधारणतया यह मान्य नहीं हो सकता, मुझे भी कैसे होता? और मैं श्री इलाचंद्र जोशी के उपकार को मानता हुआ कि उन्होंने प्रगतिवाद के चक्कर में पड़ने से पहले ही मेरी आंखे खोल दी, प्रगतिवादियों को ‘असाहित्यिक पेशेवर प्रोपैगैंडिस्ट’, ‘गड्डलिका-प्रवाह-पंथी’, ‘उच्छृंखलतावादी’, ‘धूर्त’ आदि दुर्वचनों से सुबह शाम उनकी स्तुति करता रहता। सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं या हिन्दी के अधिकांश तरुण लेखक आज इस तरह की रचनाओं के मिर्च-मसालेदार साहित्यिक खाद्य से मानसिक-भोजन प्राप्त कर साहित्य क्षेत्र में नहीं आए हैं, इस कारण प्रगतिवाद के प्रति जोशीजी की घृणा के कीटाणु हमारे दिमागों में घुसकर बीमारी नहीं फैला पाते। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि लोग कितनी सरलतापूर्वक न्यस्त-स्वार्थ मनोवृत्ति द्वारा उत्पन्न भ्रमों का प्रचार करने लगते हैं। क्योंकि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रगतिवाद द्वारा उठाई समस्याओं, उसके वक्तव्यों और उसके दृष्टिकोण को समझकर अपनी रचनात्मक आलोचना देना नहीं है, बल्कि उसपर कल्पित आरोप लगाकर ऐसे भ्रमों की सृष्टि करना है जो प्रगतिवाद को बदनाम कर दें, उसके स्वाभाविक विकास को रोक दें और वर्तमान पूंजीवादी समाज की साहित्यिक अराजकता और मानसिक विश्रृंखलता को भी ज्यों का त्यों कायम रखें। ‘प्रचारात्मकता’ के नामपर प्रगतिवाद के विरुद्ध स्वर ऊंचा करने वाले ये महाशय अपने कथनों के अर्थारोप स्वयं नहीं समझते या जानबूझकर भी वे अंजान बने हैं, अतः ‘क्या साहित्य प्रोपैगैंडा है?’ प्रश्न पर विचार करते समय हम इन प्रगतिवाद विरोधी सज्जनों के आक्षेपों और मतों पर ध्यान न देंगे क्योंकि तर्क के अभाव के कारण वे समस्या को समझने में मदद नहीं देते। इसमें संदेह नहीं है कि अधिकांश प्रगतिवादियों का यह मत रहा है कि साहित्य प्रोपैगैंडा है या प्रोपैगैंडा का साधन है, किन्तु वे प्रोपैगैंडा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में करते हैं यह स्थापना सही है या गलत इसपर हमें स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए।
‘समस्त साहित्य प्रोपैगैंडा है’ यह मत कैसे और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया और आगे चलकर किन लेखकों ने क्यों इसकी पुष्टि की, इसका क्रमबद्ध विवरण देना कठिन है और आवश्यक भी नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है रूस की क्रांति के अवसर पर यह नारा लगाया गया कि ‘साहित्य वर्गयुद्ध का एक हथियार है।’ यह एक गलत नारा था। किन्हीं खास परिस्थितियों में कोई नारा किस प्रकार उठाना चाहिए यह साधारण कार्य नहीं है क्योंकि उन परिस्थितियों की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य संगठन करने के उद्देश्य से जनसमूह को प्रेरित करने के लिए ही केवल नारा नहीं लगाया जाता – ऐसा नारा तात्कालिक आवश्यकताओं से इतना आबद्ध रहेगा कि परिस्थितियों के बदलने पर वह एकदम बेकार हो जाएगा और कदाचित नई परिस्थितियों के विपरीत पड़कर वह उनके विकास में बाधक हो उठे। भावों और विचारों में मनुष्य के मस्तिष्क में चिपके रहने की ऐसी आदत होती है कि नई तथा विपरीत परिस्थितियों उत्पन्न हो जाने पर भी उनका उन्मूलन नहीं हो पाता। अतः केवल सम-सामयिक उपयोग के नारे आगे के विकास में बाधांए भी डाल सकते हैं। सही नारा वही होता है जिसके आधार पर नई परिस्थितियों के अंदर प्रयोग में लाने के लिए नई नीति का विकास किया जा सके, अर्थात जिसमें भावी वास्तविकता की संभावनाएं अंतर्निहित हों तथा जो जनसमूह में ऐसी मिथ्या आशाएं न उत्पन्न करे जिनकी कभी पूर्ति न की जा सके। इस दृष्टि से देखने से यह नारा दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि जबतक रूस में वर्ग युद्ध था उसी समय तक उसका उपयोग भी था, यद्यपि उस अवस्था में भी उसने साहित्य और कला की समस्याओं को बहुत हल्का करके तोलने की कोशिश की थी। इस नारे को मान्य मानकर प्रत्येक लेखक के लिए यह जरूरी हो गया कि वह केवल पूंजीपति और मजदूर, श्वेत सेना या लाल सेना, जारशाही और बोल्शेविक पार्टी, कुलक और किसान के संघर्षों का, शोषित वर्गों की विजयकामना प्रकट करते हुए, ज्यों का त्यों तथा सीधा राजनैतिक वर्णन ही करे। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि इन संघर्षों का वर्णन करके उत्कृष्ट साहित्य की रचना नहीं की जा सकती; की जा सकती है और उसके उदाहरण मौजूद हैं। परन्तु वहां ऐसी कृत्रिम स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लेखक यदि मजदूर के व्यक्तिगत जीवन के प्रेम और विरह, आशा और निराशा आदि पहलुओं का वर्णन करता था तो चूंकि उसमें सीधे रूप से शोषक वर्ग पर आक्रमण न किया जाता था, इस कारण यह समझा जाने लगा कि वह वर्ग संघर्ष के हथियार को कुन्द बना रहा था। इसके अतिरिक्त इस नारे में विरासत रूप में मिले प्राचीन साहित्य के प्रति एक नकारात्मक भाव भी था जिससे सामाजिक विकास के साथ-साथ बढ़ने वाली साहित्य की ऐतिहासिक परम्पराओं का तिरस्कार किया गया, क्योंकि वे आज की क्रांति में वर्गयुद्ध का तेज हथियार न बन सकती थी। इस प्रकार इस नारे ने साहित्य और कला की उपयोगित को बहुत सीमित करके देखा। फलतः इस नारे को अपनाकर लेखकों की संस्था त्।च्च् ने रूस के लेखकों पर अनेक प्रतिबंध लगाए, जिसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रोलेतेरियन (श्रमजीवी) साहित्य प्रोपैगैंडा प्रधान हो गया। गोर्की, स्टालिन तथा अन्य कई लेखकों ने इस गलत नारे का अनुभव किया और त्।च्च् तोड़ दी गई और लेखकों का एक नया संगठन बनाया गया जिसने ‘समाजवादी’ यथार्थवाद का (समाजवादी रोमैंटिसिज्म भी जिसके अंतर्गत है) नारा बुलंद किया। समाजवादी यथार्थवाद साहित्य के एक विशिष्ट दृष्टिकोण और उसकी एक विशिष्ट शैली का द्योतन करता है अर्थात वह साहित्य या कला की वस्तु और रूप योजना दोनों को घेर लेता है। इसके अतिरिक्त उसमें प्राचीन साहित्य की सजीव परम्पराओं को ग्रहण करने, नई परिस्थितियों के अनुकूल उसका विकास करने एवं कला एवं साहित्य को एक ऐसा मार्ग देने की संभावनाएं मौजूद हैं जिसकी अगली मंजिलें भविष्य के गर्भ में हैं। किन्तु अब तक ‘साहित्य प्रोपैगैंडा है’ का नारा विस्मृत नहीं हो सका है और आवेश में आकर हमारे लेखक इसे दुहराते जाते हैं यहां तक कि अमेरिका के प्रसिद्ध माक्र्सवादी लेखक जोजेफ फ्रीमेन ने भी ‘संयुक्तराष्ट्र में श्रमजीवी साहित्य’ पुस्तक की भूमिका में एक स्थान पर कुछ ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि ‘कला का, जो वर्ग युद्ध का एक साधन यंत्र है, मजदूर वर्ग को अपने एक हथियार के रूप में विकास करना चाहिए।’ उनका कहना है कि कला ‘अनुभव का विनिमय’ करती है। लेकिन ‘अनुभव’ शब्द के अंदर उसकी पकड़ छिपी है। पूंजीवादी विचारक या आलोचक मजदूर वर्ग के जीवन की अभिव्यंजना को अनुभव के अंतर्गत नहीं मानते। बल्कि किसी स्त्री के उरोजों की उपमाओं से भरे वाक्य चमत्कारों को ही अनुभव मानते हैं। फ्रीमेन के पूरे लेख को पढ़ने से यह धारणा तो निर्मूल हो जाती है कि वे इस नारे के अर्थ में साहित्य को वर्गयुद्ध का हथियार मानते हैं। फ्रीमेन का केवल यह कहना है कि साहित्य का प्रयोग चूंकि पूंजीपति वर्ग अपने स्वार्थों की रक्षा के निमित्त कर रहा है, ऐसी दशा में श्रमजीवी वर्ग को भी उसका उपयोग अपने हितों की रक्षा और संघर्ष के विकास में करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि समूचा साहित्य वर्गयुद्ध का हथियार है अथवा उसे होना चाहिए। तो भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग यदि सावधानी से किया जाए तो अच्छा है। यद्यपि इससे, खेद है, हमारे बहुत से पूंजीवादी आलोचकों की मौके-बेमौके फतवा देने की रोजी छिन जाएगी।
चूंकि योरप के अन्य देशों में वर्गयुद्ध एक सफल क्रांति का रूप धारण न कर पाया अतः वहां साहित्य को वर्गयुद्ध का हथियार घोषित करने की उतनी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई जितनी प्रचार का साधन बनाने की, जिससे मजदूर वर्ग का संगठन किया जा सके, उसके अंदर समाजवाद और क्रांति की चेतना फैलाई जा सके। शायद इसीलिए वहां किसी ने यह नारा ईजाद किया कि साहित्य प्रोपैगैंडा है या होता है। पाठकों ने संभव है अमेरिका के प्रसिद्ध समाजवादी उपन्यासकार अप्टन सिंक्लेयर की पुस्तक डंउउवदंतज पढ़ी हो। आलोचना साहित्य की दृष्टि से पुस्तक निम्नकोटि की है और वह प्रगतिवाद के समीक्षा सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन उसमें प्रारम्भ से लेकर रूस की समाजवादी क्रांति तक के योरप और अमेरिका के सभी महान लेखकों और कलाकारों की कृतियों का मूल्यांकन इस दृष्टिकोण को सामने रखकर ही किया गया है कि वे अपने समय के किसी न किसी वर्ग की भावनाओं का प्रोपैगैंडा करती थीं। अप्टन सिंक्लेयर के अनुसार समस्त साहित्य प्रोपैगैंडा है, सार्वभौम तथा अनिवार्य रूप से, कभी अज्ञात रूप से अन्यथा अधिकतर ज्ञात रूप से। कला जीवन की अभिव्यक्ति है जो कलाकार के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है और उसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करना और उन्हें भाव, विश्वास और कार्य परिवर्तन के लिए प्रेरित करना होता है। महान कला का जन्म तभी होता है जब जीवंत तथा महत्वपूर्ण प्रोपैगैंडा कलात्मक नैपुण्य के साथ किसी कला विशेष के माध्यम द्वारा किया जाता है। सिंक्लेयर का कहना केवल इतना है कि यह दावा करना कि कला में प्रोपैगैंडा को स्थान नहीं है अथवा कला का स्वतंत्रता और न्याय की भावनाओं से कोई संबंध नहीं है, एक प्रवंचना है, एक ऐसा भ्रम है जिसे न्यस्त स्वार्थ वाले वर्गों ने फैला रखा है। इसके विपरीत उनके अनुसार कला में प्रोपैगैंडा ही प्रधान प्रेरणा है। क्योंकि साहित्य और कला की प्रत्येक रचना किसी न किसी भाव, विचार, विश्वास या दृष्टिकोण को व्यक्त करती है, और चूंकि अब तक समाज दो या दो से अधिक परस्पर-विरोधी वर्गों में बंटा रहा है, इस कारण यह भाव, विचार, विश्वास या दृष्टिकोण किसी न किसी वर्ग के अनुकूल या प्रतिकूल अवश्य रहते हैं और जब तक मनुष्य वर्गहीन समाज नहीं बना लेता तब तक कला-साहित्य का प्रधान गुण प्रोपैगैंडा ही रहेगा। यदि सिंक्लेयर की प्रोपैगैंडा की इतनी व्यापक व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो प्रोपैगैंडा को कला और साहित्य का एक हद तक सामान्य गुण कहा जा सकता है, पर केवल एक हद तक ही।
सामान्यतः जो लोग आजकल प्रगतिवादियों पर प्रोपैगैंडा के नाम से दोष मढ़ते हैं, वे प्रोपैगैंडा के इतने ही व्यापक अर्थ समझते हैं यद्यपि उसका जो पहलू प्राचीन साहित्य और पूंजीवादी साहित्य पर लागू होता है उसे मानने को तैयार नहीं होते। इन व्यापक अर्थों में प्रोपैगैंडा शब्द से शायद पुराने लेखक और कलाकार इतना न चिढ़ते, वे शायद इस स्वीकार भी कर लेते।
वीरगाथा काल के कवियों को यह स्वीकार करने में क्या संकोच होता कि वे अपने शासक या नरेश के वैभव और पराक्रम की गाथाएं लिखकर उनका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, और क्या यह प्रोपैगैंडा न हुआ? आल्हा, पृथ्वीराजरासो तथा तत्कालीन काव्यग्रंथों में क्या प्रोपैगैंडा नहीं है? और यह बात भी नहीं है कि चंदबरदाई को निम्नकोटि का कवि समझा जाता हो। इसी प्रकार भक्तिकालीन कवियों ने वैष्णव तथा सूफी मतों का प्रचार किया था। तुलसीदास जी की रामायण में ऐसे कितने स्थल नहीं है जहां उन्होंने पाठकों की राम की भक्ति और उपासना के लिए प्रेरित किया है और राम से विमुख जाने वालों के लिए रौरव नरक की भीषण यातनाओं की तस्वीर खींची है।
तुलसीदासजी के इस वर्णन को प्रोपैगैंडा न मानकर यदि ‘शाश्वत सत्य’ मान लिया जाए तो मुझे भय है कि आजकल के भौतिकवादी युग में रौरव-नरक के बन्दियों की संख्या इतनी बढ़ गई होगी कि यमराज को ब्रिटिश सरकार की तरह ‘डिटेन्शन कैम्प’ खुलवाने पड़ रहे होंगे!
मीरा और सूरदास के पदों में भी प्रचार की मात्रा कम नहीं है। फिर भूषण तो, जिन्हें हमारे आलोचक महाकवि स्वीकार करते हैं, यद्यपि यह विवादास्पद है, अपन रचनाओं में खुलेआम महाराज शिवाजी का प्रोपैगैंडा करते थे। उनकी शिवा-बावन आदि से अन्त तक प्रोपैगैंडा प्रधान है। इसी प्रकार आधुनिक लेखकों की रचनाओं में किसी वर्ग या सम्प्रदाय का प्रोपैगैंडा साबित किया जा सकता है। प्रेमचन्द, शरतचन्द्र, टैगोर और इकबाल की कृतियों में भी, जो इस युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हुए हैं, प्रोपैगैंडा की कमी न मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दृष्टिकोण से देखने से कला और साहित्य-कृतियों में प्रोपैगैंडा दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है। पुराने जमाने में लेखक इसे स्वीकार करने से कभी इन्कार न करते, क्योंकि वे इस बात से इन्कार न कर सकते थे कि साहित्य और समाज में अविच्छिन्न संबंध है या कि साहित्य समाज का एक अंग है और वह जीवन की अभिव्यंजना करता है – यद्यपि साहित्य के उपयोग और उद्देश्य के बारे में किसी सामाजिक दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्य आंकने की भाषा से वे अवगत न थे। किन्तु आज के लेखक अक्सर इसे स्वीकार नहीं करते। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि कलाकार समाज की क्रियाशीलता से इतना दूर हो गया है कि उसके मस्तिष्क में ‘कला कला के लिए’ की भ्रामक पूंजीवादी धारणा ने स्थान जमा लिया है। दूसरा यह कि आज वर्ग-संघर्ष इतना तीव्र हो गया है कि इसे स्वीकार करने का अर्थ है कि या जो लेखक यह मान ले कि वह पूंजीपति वर्ग का प्रोपैगैंडा करता है, जो कि एक श्रेष्ठ लेखक कभी कहना मंजूर न करेगा क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उसका भी शोषण कर रखा है, या फिर वह यह स्वीकार कर ले कि वह श्रमजीवी वर्ग का प्रोपैगैंडा करता है, जो कि कहना उसके लिए अनेक कष्टों और यातनाओं और अभिजात वर्ग की उपेक्षा और निन्दा का कारण हो सकता है। अतः आज लेखक ‘संघर्ष से परे रहने’ या तटस्थ रहने का उपक्रम करता है यद्यपि वह ऐसा कर नहीं पाता। विगत युगों के लेखक इस प्रकार दो परस्पर-विरोधी अवस्थाओं से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व से बचे रहते थे। उन युगों में वर्गों का संघर्ष अपने ऐतिहासिक विकास की उस प्रारम्भिक अथवा मध्य अवस्था में था जब लेखक या कलाकार के सामने दो में से एक वर्ग का दामन पकड़ना अनिवार्य न हो गया था। अतः प्र्र्र्रगतिवादियों ने यदि कभी साहित्य को प्रोपैगैंडा माना है तो इसी अर्थ में, किसी दूसरे अर्थ में नहीं। यहां यह बात विचारणीय है कि हमारे ये कतिपय आलोचक चन्दबरदायी या भूषण की कविता में अथवा अपनी रचनाओं में व्यक्त उद्गारों में किसी वर्ग का प्रोपैगैंडा नहीं देखते। यदि कोई राजकुमारों और राजकुमारियों, कोमलांगियों और सूटबूटधारी पुरुषों के विषय में लिखता है तो वह उनकी दृष्टि में प्रोपैगैंडा नहीं है किन्तु यदि कोई किसान मजदूर या मुफलिसों की बस्तियों के बारे में लिखता है तो वह प्रोपैगैंडा है। अतः यदि कुछ आलोचक प्रगतिवादियों पर यह आरोप लगाते हैं कि वे समीक्षा सिद्धांतों को तिलांजलि देकर प्राचीन-साहित्य अथवा आधुनिक-साहित्य के अन्दर शासक वर्गों की भावनाओं की अभिव्यक्ति ढूंढ़कर उसे प्रोपैगैंडा कहते हैं तो प्रगतिवादी भी न्यायपूर्वक उनपर आरोप लगा सकते हैं कि वे प्रगतिवादी साहित्य को प्रोपैगैंडा कहते हैं। और खेद इस बात का है कि साहित्य-समीक्षा की प्रणाली की अवहेलना पर रोष प्रकट करने वाले ये आलोचक ही उस प्रणाली को तिरस्कार करने का सबसे पहला अपराध करते हैं। प्रगतिवादी यदि पूंजीवादी वर्ग के प्रोपैगैंडा का आरोप करते हैं तो आलोचक मजदूर वर्ग के प्रोपैगैंडा का। प्रगतिवादियों में कम से कम इतनी ईमानदारी तो अवश्य है कि समस्त साहित्य को प्रोपैगैंडा करकर वे समस्त साहित्य की राशि में शामिल अपने साहित्य को भी प्रोपैगैंडा स्वीकार करते हैं, तथा प्रोपैगैंडा को अपने में एक बुरी चीज नहीं मानते, यदि बुरा मानते हैं तो केवल शोषक वर्गों के प्रोपैगैंडा को, क्योंकि वह शोषण के कायम रखने का साधन बनता है। इसके विपरीत प्रगतिवादियों के विरोधी प्रोपैगैंडा को हेय मानते हैं, लेकिन पूंजीपति वर्ग की भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोपैगैंडा नहीं मानते; उन्हें मनुष्य की शाश्वत भावनाएं मानते हैं, और मजदूर वर्ग की भावनाओं को प्रोपैगैंडा कहते हैं अर्थात उसे हेय समझते हैं। लेकिन यह तो एक विवाद की बात हुई। वास्तव में क्या सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है? यदि सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है तो निश्चय ही पूंजीपति वर्ग की अपेक्षा मजदूर वर्ग का प्रोपैगैंडा ज्यादा अच्छा है।
अमेरिका के एक दूसरे प्रसिद्ध आलोचक-उपन्यासकार जेम्स.टी.फेरेल ने, जो समाजवादी हैं, अपनी पुस्तक । छवजम वद स्पजमतंतल ब्तपजपबपेउ में इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि हमें सबसे पहले प्रोपैगैंडा शब्द की व्याख्या निश्चित कर लेनी चाहिए। लेनिन की पुस्तक ॅींज प्े ज्व ठम क्वदमघ् से एक उद्धरण देकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि प्रोपैगैंडा किन्हीं सिद्धांतों, योजनाओं तथा विचारों का प्रचार होता है ताकि किसी प्रोगैम या कार्यक्रम के अनुसार शीघ्र ही अमल किया जा सके। फेरेल का कथन है कि यदि इस व्याख्या को स्वीकार किया जाय तो साहित्य को प्रोपैगैंडा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माक्र्स का ‘कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो’ प्रोपैगैंडा की चीज होकर भी न केवल विचार-परिपाक का सुन्दर नमूना है, बल्कि एक श्रेष्ठ साहित्यिक रचना भी है; इसके विपरीत आन्द्रे मालरो का उपन्यास डंदश्े थ्ंजम यद्यपि एक उत्कृष्ट रचना है तथापि प्रोपैगैंडा की दृष्टि से उसके विचार विवादास्पद हैं। अतः साहित्य और प्रोपैगैंडा दो भिन्न चीज है, यद्यपि दोनों का किसी भी रचना में सम्मिश्रण भी होता रहता है। फेरेल ने इससे यह सिद्ध किया है कि साहित्य के अपने अलग नियम होते हैं जिनसे उसको उत्कृष्टता का अन्दाजा लगाया जाता है। साहित्य में केवल सामयिक तत्व ही नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो उसे सापेक्ष्य स्थायित्व का गुण प्रदान करते हैं। अतः फेरेल की राय है कि ‘सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है’ इस नारे को त्याग देना चाहिए और उसके स्थान पर ‘साहित्य सामाजिक प्रभाव का अस्त्र है’ रखना चाहिए।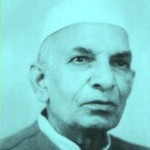
जेम्स टी.फेरेल से मैं कहां तक सहमत हूं, यह ज्यादा महत्व की बात नहीं है, यद्यपि यह स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं फेरेल द्वारा की गई प्रोपैगैंडा की व्याख्या से सहमत हूं। महत्व की बात यह प्रश्न है कि साहित्य की ऐसी समाज-शास्त्रीय व्याख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये व्याख्याएं चाहे जितनी सर्वमान्य क्यों न हों, कहां तक साहित्य की परिभाषा के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं, अर्थात कहां तक वे हमें साहित्य का मूल्यांकन करने में सहायता देती हैं, अतः हमारे समीक्षा-शास्त्र के अन्तर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं। श्री सुमित्रानन्दन पंत की ‘पल्लव’ की भूमिका का यह वाक्य कि ‘हम ब्रज की जीर्ण-शीर्ण छिद्रों से भरी पुरानी छीट की चोली नहीं चाहते, इसकी संकीर्ण कारा में बन्द हो हमारी आत्मा वायु की न्यूनता के कारण सिसक उठती है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है’ विचारणीय है। इस वाक्य की शैली चाहे कितनी ही अलंकृत और पुरानी क्यों न लगे – या अनुपयुक्त भी कह सकते हैं – लेकिन यह समीक्षा प्रणाली के एक नए विकास की ओर अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश करता है। पहले जब सामंती काल में कविता मनोरंजन या आनन्द प्रदान करने के लिए लिखी जाती थी, तब कविता का ‘उद्देश्य’ रस का उद्रेक करना था। और समाज का संगठन ऐसा था कि कविता या साहित्य के ‘उपयोग’ का कभी प्रश्न ही नहीं उठता था। ‘उद्देश्य’ के अन्दर ही ‘उपयोग’ शामिल था, अर्थात दोनों को एक ही मान लिया गया था। और इस ‘उद्देश्य’ या उसमें शामिल ‘उपयोग’ की सीमाएं बहुत संकीर्ण थीं। इस कारण इस ‘उद्देश्य’ की प्राप्ति के लिए इसी सीमित परिधि के अन्दर प्रयोग किये जाते थे और इन प्रयोगों को सफल बनाने के प्रधान अस्त्र थे: अलंकार, ध्वनि, शब्द शक्तियां, वक्रोक्ति, गुण आदि। जहां तक समाजशास्त्र, दर्शन या मनोविज्ञान का संबंध था, उनके अपने अलग बाड़े थे, और यह आवश्यक न समझा जाता था कि इन सब बाड़ों में यातायात की आवश्यकता है। यह रीतिकाल की बात है। उसके पहले भी भक्तिकाल में जब काव्य की आत्मा के स्थान पर धर्म और नैतिकता विराजमान थे आलोचना-पद्धति किसी सामाजिक दृष्टिकोण का अवलम्ब लेकर काव्य का मूल्यांकन नहीं करती थी। छन्दशास्त्र और अलंकारशास्त्र, ये ही इस काव्य-समीक्षा रथ के दो पहिये थे; और रसवाद का सिद्धांत उसके लक्ष्य या उद्देश्य की ओर एक अस्पष्ट इशारा मात्र करता था। भाव या रूप के ‘सौंदर्य’ का कुछ नियमों के अनुसार निरूपण करना ही शास्त्रीय समीक्षा का उद्देश्य था। काल-स्थित समाज में काव्य या साहित्य का क्या उपयोग है, और उसके अनुकूल उसका क्या उद्देश्य है, अर्थात उसका संविधायक पहलू क्या है, इस ओर किसी का ध्यान न जाता था मानो ये प्रश्न साहित्य या कला के मूल्यांकन में असंगत हों, और न कविता या साहित्य की सृष्टि के मानसिक उद्गम तक पहुंचने की कोशिश होती थी, अर्थात मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता न समझी जाती थी – सत्य तो यह है कि यह शास्त्र उस समय न हमारे यहां था और न योरप में ही। अतः कुछ मनस्थितियों या मनोविकारों के वर्णन तक ही समीक्षा सीमित थी, जिसमें श्रृंगार या वात्सल्य, वीर या रौद्र, अद्भुत या वीभत्स, करुण या हास्य रसों के, जो मनस्थितियों का अनुपयुक्त द्योतन करते हैं, परिपाक को दिखाकर विश्रांति ले ली जाती थी। इस प्रकार हमारी प्राचीन समीक्षा-प्रणाली का क्षेत्र इतना संकीर्ण था कि समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक-विश्लेषणशास्त्र के विकास के साथ – यद्यपि इन दोनों शास्त्रों का विकास योरप में हुआ – उसकी संकीर्ण सीमाओं का टूटना आवश्यक हो गया, और कविता या साहित्य जो अब तक प्राचीन समीक्षाशास्त्र की श्रृंखलाओं में जकड़ा था, उसको भी नए ज्ञान के साथ अपना सीमा-विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर पंतजी के उद्धरण को देखें तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ब्रज-काव्य-प्रणाली की ‘संकीर्ण कारा में बन्द हो’ ‘वायु की न्यूनता’ से ‘आत्मा का सिसक उठना’ और ‘शरीर का विकास रुक जाना’ इस अनुभूति का द्योतक है कि काव्य और साहित्य का विकास तब तक रुका रहेगा जब उसका सीमा-विस्तार नहीं किया जाता; और यह सीमा विस्तार समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के नए दृष्टिकोण का भी सूचक है, कि समीक्षाशास्त्र को भी ‘छीट की चोली’ का रंग-बिरंगापन ही नहीं देखना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ‘वायु की न्यूनता’ से आत्मा और शरीर का विकास तो नहीं रुकता। इस सांकेतिक शब्दावली को हटा दें तो इसका अर्थ है कि काव्य और साहित्य के उद्देश्य और उपयोग को हमें फिर से जांचना चाहिए और उनके जांचने के लिए हमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के मापदण्डों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह कि समाजशास्त्र के मापदण्डों से मूल्यांकन करने की प्रथा का श्रीगणेश प्रगतिवादियों के पहले ही शुरू हो गया था। साहित्य के संविधायक पहलू से उसपर विचार किया जाने लगा था। और ‘सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है’, साहित्य के इसी संविधायक दृष्टिकोण का एक उत्तर है। लेकिन यहां हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सारे साहित्य को प्रोपैगैंडा या सामाजिक-प्रभाव का अस्त्र कहकर आज के समाज में उसके एक महत्वपूर्ण संविधायक पहलू का ही निर्देश किया जाता है, और केवल इस दृष्टि से खरी उतरनेवाली कोई रचना अपने में श्रेष्ठ नहीं हो जाती। उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते समय उसकी सौंदर्यानुभूति, उसकी रूपयोजना, शैली और प्रौढ़ता, वाक्य-रचना, शब्द-प्रयोग आदि अनेक दूसरी कसौटियों पर भी उसे कसना आवश्यक है, और प्रगतिवादी इन सब कसौटियों पर भी काव्य या साहित्य-कृति का कसना आवश्यक समझते हैं, उनके महत्व को जानते हैं, यद्यपि आज के संक्रमण-काल में वे साहित्य के संविधायक पहलू को दृष्टि में रखकर उसका सामाजिक दृष्टिकोण से विवेचन करना अधिक आवश्यक समझते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला तो यह कि आज के समाज में कला साहित्य का उपयोग अनेक राजनीतिक और आर्थिक हितों को दृष्टि में रखकर किया जा रहा है, और जो समाज-व्यवस्था को बदलने में संलग्न शक्तियां हैं वे कला-साहित्य के प्रभाव को समझकर भी उन्हें विश्वव्यापी संघर्ष में प्रगतिशील शक्तियों के शक्ति-वर्धन का साधन न बनाए यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण न होगा – यह भाव कला या साहित्य के प्रति अवज्ञा या उपेक्षा का सूचक नहीं है वरन उनके महत्व और उनकी शक्ति के प्रति स्वीकृति का द्योतक है; न यह भाव इस बात का सूचक है कि प्रगतिवादी कला और साहित्य के सौंदर्यगत मूल्य की कद्र नहीं समझते; और न इसका अर्थ है कि प्रगतिवादी साहित्य के संविधायक पहलू पर जोर देकर लेखकों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि कलात्मक दृष्टि से उनकी रचनाएं चाहे कुछ न हो लेकिन आज की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर उनके वक्तव्य चैकस होने चाहिए। दूसरा यह कि प्रगतिवादी यह जानते हैं कि केवल रचना कौशल के कारण ही, और वाक्य-विन्यास या शैली और कला के कारण ही कोई रचना श्रेष्ठ नहीं बन सकती, न पहले कभी बनी – चाहे तब समीक्षक इस पहलू से अवगत न हों, या उसे आवश्यक न समझते हों – न आज बन सकती है, और उसका मूल्यांकन करने के लिए उसके सामाजिक दृष्टिकोण को जांचना भी आवश्यक है, अर्थात कला या साहित्य को सामाजिक उद्देश्य और उपयोग से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों उसके आवश्यक अंग हैं। प्रगतिवादियों पर यदि किसी बात का न्यायोचित आरोप किया जा सकता है तो केवल इस बात का कि वे कला और साहित्य के सामाजिक दृष्टिकोण अर्थात उसके उद्देश्य और उपयोग को ठीक-ठीक स्पष्ट रूप से आंक लेना चाहते हैं और कोरी वायवी, या काल्पनिक, या आदर्शवादी, भावुकता-प्रधान स्थापनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। साहित्य को इतने विस्तृत चैखटे के अन्दर रखकर देखने का प्रयत्न तो अभी शुरू हुआ है, अतः प्रगतिवादी इस नए दृष्टिकोण को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने की ओर प्रयत्नशील हैं, अभी या कभी वे अंतिम निर्णय पर पहुंच जायेंगे, ऐसा कोई भ्रम उन्हें नहीं है। लेकिन सत्य को अधिकाधिक प्राप्त करने का एकमात्र यही तो तरीका है कि हम नित नए अनुभव से अपनी स्थापनाओं को समृद्ध बनाते जांय।
इन विचारों की दृष्टि में यदि हम पुनः ‘क्या साहित्य प्रोपैगैंडा है?’ प्रश्न को जांचें तो हमें उसपर नई रोशनी पड़ती दिखाई देगी। ‘सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है’ की स्थापना को अब हम आसानी से अस्वीकृत कर सकते हैं। क्योंकि इस स्थापना में प्रोपैगैंडा की व्याख्या के अनुसार प्रोपैगैंडा और प्रतिपादन को पर्याय मान लिया गया है। लेकिन योजना पर अमल करने या अमल कराने के लिये जनसमूह या उसके किसी अंग को प्रेरित करना एक चीज है और व्यक्ति या समूह के विचारों या भावनाओं का प्रतिपादन करना एक दूसरी चीज है। पहला प्रोपैगैंडा है, दूसरा प्रोपैगैंडा नहीं है। यदि साहित्य में अनिवार्यतः विचारों या भावनाओं का प्रतिपादन मिलता है तो उसे प्रोपैगैंडा नहीं कहा जा सकता। यह दूसरी बात है कि सामाजिक क्रियाशीलता की अभिव्यंजना का साहित्य पाठक को भी उसकी अनुभूति कराता है पर इससे वह प्रोपैगैंडा का पर्याय नहीं बन जाता। लेकिन फेरेल की यह स्थापना उपयुक्त नहीं है कि ‘साहित्य सामाजिक प्रभाव का अस्त्र है।’ यह एक स्वयं सिद्धि है उस तरह की कि आदमी बुद्धि-धारी जानवर है, और अस्त्र जोड़ देने से वह स्वयं सिद्धि न तीव्र हो जाती है न प्रभावपूर्ण। उसके स्थान पर ‘साधन’ ‘चीज’ आदि भी उपयुक्त रहते। इसके अतिरिक्त ‘सामाजिक प्रभाव’ बड़ा कमजोर वाक्यांश है, क्योंकि ‘प्रभाव’ शब्द को सीधे तौर पर सामाजिक प्रगति की अपेक्षा में मापना कठिन है और इस सामाजिक प्रगति में इस प्रभाव की क्या सक्रिय भूमिका रहती है इसका बहुत क्षीण आभास इस शब्द से मिलता है। जिस क्रांतिकारी युग में हम रहते हैं, उसकी वास्तविकता के मुकाबले में यह अभिव्यक्ति अत्यंत लचर है। फिर साहित्य केवल सामाजिक प्रभाव का अस्त्र नहीं है, वह सामाजिक परिवर्तन का भी अस्त्र है। सामाजिक परिवर्तन में साहित्य वह भाव-प्रधान सामाजिक शक्ति उत्पन्न करता है जो मनुष्य के भाव-जगत को परिवर्तित कर इतना विस्तृत बना देती है कि वह हमारे अंदर देखने और अनुभव करने की क्षमता पैदा कर हमें विगत तथा पुरातन के विकसित परिवर्तित रूप आगत तथा नवीन को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है। भाव-जगत का यह परिवर्तन भौतिक जीवन की आवश्यकताओं से प्रभावित होता है और पुनः वह भौतिक जीवन को बदलकर एक उच्च धरातलपर संगठित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह भाव-जगत की क्रिया-प्रक्रिया मनुष्य की स्वतंत्रता प्राप्त करने की जीवन-क्रिया का एक अनिवार्य अंग है। श्रेष्ठ साहित्य इस क्रिया में सहायक होता है, सहायक ही नहीं उसका साधन भी बनता है। श्रेष्ठ कला या साहित्य का यह गुण है। अतः यदि हमें साहित्य की कोई संविधायक स्थापना करनी ही है और यह कहना मुश्किल है कि आज की संघषपूर्ण परिस्थिति में उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, तो हमें स्वर्गीय काॅडवेल की स्थापना स्वीकार करनी चाहिए कि ‘साहित्य या कला मनुष्य की स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक साधन है।’ इसमें ‘स्वतंत्रता’ शब्द विवादास्पद है अवश्य, और उसका उत्तर विज्ञान और दर्शन देने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उसमें अन्य स्थापनाओं के दोष नहीं हैं, और उत्कृष्ट कला या साहित्य के प्रति तो असीम श्रद्धा का भाव है।
प्रोपैगैंडा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हो सकता है, हुआ है, और आज भी होता है। प्रगतिवादियों ने जब कभी भी उसका प्रयोग किया है, तब ऐसे सामान्य अर्थ में कि उससे किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य को प्रोपैगैंडा कहकर उन्होंने उसके उत्कृष्ट भावना प्रधान, कल्पनात्मक और कलात्मक गुणों की अवहेलना नहीं की, न उनका बहिष्कार ही आवश्यक समझा है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मैं साहित्य की इस व्याख्या से सहमत हूं अथवा यह दृष्टिकोण सही है – इसका विवेचन मैं आगे करुंगा। किन्तु जोशीजी और उनकी तरह सोचनेवाले आक्षेपकर्ता, खेद है, प्रगतिवादियों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश न कर उसे ऐसे भद्दे अर्थ पहना देते हैं कि वह निन्दनीय दीख उठता है। मुझे यह स्वीकार करने में जरा भी आपत्ति नहीं कि यदि मुझे इन लोगों के लेखों द्वारा ही प्रगतिवाद के दृष्टिकोण से परिचय मिलता, तो मैं उसे इतना वीभत्स और कुत्सित, प्रगतिविरोधी और असाहित्यिक समझता कि मुझे अनायासही प्रगतिवाद से घृणा हो जाती। मैं समझता कि प्र्रगतिवाद कला और साहित्य की कलात्मकता और साहित्यिकता तथा अन्य सभी उन गुणों को जो इन्हें सजीव, मधुर और सुन्दर बनाते हैं, नष्ट कर उनके स्थानपर नीरस ‘वादों’ की व्याख्या, हड़ताल करने के ऐलान और मजदूर-किसान सभाएं या अन्य पार्टियां संगठित करने के प्रोगैम और प्रदर्शनों में गाने योग्य गीत भरना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को साधारणतया यह मान्य नहीं हो सकता, मुझे भी कैसे होता? और मैं श्री इलाचंद्र जोशी के उपकार को मानता हुआ कि उन्होंने प्रगतिवाद के चक्कर में पड़ने से पहले ही मेरी आंखे खोल दी, प्रगतिवादियों को ‘असाहित्यिक पेशेवर प्रोपैगैंडिस्ट’, ‘गड्डलिका-प्रवाह-पंथी’, ‘उच्छृंखलतावादी’, ‘धूर्त’ आदि दुर्वचनों से सुबह शाम उनकी स्तुति करता रहता। सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं या हिन्दी के अधिकांश तरुण लेखक आज इस तरह की रचनाओं के मिर्च-मसालेदार साहित्यिक खाद्य से मानसिक-भोजन प्राप्त कर साहित्य क्षेत्र में नहीं आए हैं, इस कारण प्रगतिवाद के प्रति जोशीजी की घृणा के कीटाणु हमारे दिमागों में घुसकर बीमारी नहीं फैला पाते। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि लोग कितनी सरलतापूर्वक न्यस्त-स्वार्थ मनोवृत्ति द्वारा उत्पन्न भ्रमों का प्रचार करने लगते हैं। क्योंकि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रगतिवाद द्वारा उठाई समस्याओं, उसके वक्तव्यों और उसके दृष्टिकोण को समझकर अपनी रचनात्मक आलोचना देना नहीं है, बल्कि उसपर कल्पित आरोप लगाकर ऐसे भ्रमों की सृष्टि करना है जो प्रगतिवाद को बदनाम कर दें, उसके स्वाभाविक विकास को रोक दें और वर्तमान पूंजीवादी समाज की साहित्यिक अराजकता और मानसिक विश्रृंखलता को भी ज्यों का त्यों कायम रखें। ‘प्रचारात्मकता’ के नामपर प्रगतिवाद के विरुद्ध स्वर ऊंचा करने वाले ये महाशय अपने कथनों के अर्थारोप स्वयं नहीं समझते या जानबूझकर भी वे अंजान बने हैं, अतः ‘क्या साहित्य प्रोपैगैंडा है?’ प्रश्न पर विचार करते समय हम इन प्रगतिवाद विरोधी सज्जनों के आक्षेपों और मतों पर ध्यान न देंगे क्योंकि तर्क के अभाव के कारण वे समस्या को समझने में मदद नहीं देते। इसमें संदेह नहीं है कि अधिकांश प्रगतिवादियों का यह मत रहा है कि साहित्य प्रोपैगैंडा है या प्रोपैगैंडा का साधन है, किन्तु वे प्रोपैगैंडा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में करते हैं यह स्थापना सही है या गलत इसपर हमें स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए।
‘समस्त साहित्य प्रोपैगैंडा है’ यह मत कैसे और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया और आगे चलकर किन लेखकों ने क्यों इसकी पुष्टि की, इसका क्रमबद्ध विवरण देना कठिन है और आवश्यक भी नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है रूस की क्रांति के अवसर पर यह नारा लगाया गया कि ‘साहित्य वर्गयुद्ध का एक हथियार है।’ यह एक गलत नारा था। किन्हीं खास परिस्थितियों में कोई नारा किस प्रकार उठाना चाहिए यह साधारण कार्य नहीं है क्योंकि उन परिस्थितियों की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य संगठन करने के उद्देश्य से जनसमूह को प्रेरित करने के लिए ही केवल नारा नहीं लगाया जाता – ऐसा नारा तात्कालिक आवश्यकताओं से इतना आबद्ध रहेगा कि परिस्थितियों के बदलने पर वह एकदम बेकार हो जाएगा और कदाचित नई परिस्थितियों के विपरीत पड़कर वह उनके विकास में बाधक हो उठे। भावों और विचारों में मनुष्य के मस्तिष्क में चिपके रहने की ऐसी आदत होती है कि नई तथा विपरीत परिस्थितियों उत्पन्न हो जाने पर भी उनका उन्मूलन नहीं हो पाता। अतः केवल सम-सामयिक उपयोग के नारे आगे के विकास में बाधांए भी डाल सकते हैं। सही नारा वही होता है जिसके आधार पर नई परिस्थितियों के अंदर प्रयोग में लाने के लिए नई नीति का विकास किया जा सके, अर्थात जिसमें भावी वास्तविकता की संभावनाएं अंतर्निहित हों तथा जो जनसमूह में ऐसी मिथ्या आशाएं न उत्पन्न करे जिनकी कभी पूर्ति न की जा सके। इस दृष्टि से देखने से यह नारा दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि जबतक रूस में वर्ग युद्ध था उसी समय तक उसका उपयोग भी था, यद्यपि उस अवस्था में भी उसने साहित्य और कला की समस्याओं को बहुत हल्का करके तोलने की कोशिश की थी। इस नारे को मान्य मानकर प्रत्येक लेखक के लिए यह जरूरी हो गया कि वह केवल पूंजीपति और मजदूर, श्वेत सेना या लाल सेना, जारशाही और बोल्शेविक पार्टी, कुलक और किसान के संघर्षों का, शोषित वर्गों की विजयकामना प्रकट करते हुए, ज्यों का त्यों तथा सीधा राजनैतिक वर्णन ही करे। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि इन संघर्षों का वर्णन करके उत्कृष्ट साहित्य की रचना नहीं की जा सकती; की जा सकती है और उसके उदाहरण मौजूद हैं। परन्तु वहां ऐसी कृत्रिम स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लेखक यदि मजदूर के व्यक्तिगत जीवन के प्रेम और विरह, आशा और निराशा आदि पहलुओं का वर्णन करता था तो चूंकि उसमें सीधे रूप से शोषक वर्ग पर आक्रमण न किया जाता था, इस कारण यह समझा जाने लगा कि वह वर्ग संघर्ष के हथियार को कुन्द बना रहा था। इसके अतिरिक्त इस नारे में विरासत रूप में मिले प्राचीन साहित्य के प्रति एक नकारात्मक भाव भी था जिससे सामाजिक विकास के साथ-साथ बढ़ने वाली साहित्य की ऐतिहासिक परम्पराओं का तिरस्कार किया गया, क्योंकि वे आज की क्रांति में वर्गयुद्ध का तेज हथियार न बन सकती थी। इस प्रकार इस नारे ने साहित्य और कला की उपयोगित को बहुत सीमित करके देखा। फलतः इस नारे को अपनाकर लेखकों की संस्था त्।च्च् ने रूस के लेखकों पर अनेक प्रतिबंध लगाए, जिसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रोलेतेरियन (श्रमजीवी) साहित्य प्रोपैगैंडा प्रधान हो गया। गोर्की, स्टालिन तथा अन्य कई लेखकों ने इस गलत नारे का अनुभव किया और त्।च्च् तोड़ दी गई और लेखकों का एक नया संगठन बनाया गया जिसने ‘समाजवादी’ यथार्थवाद का (समाजवादी रोमैंटिसिज्म भी जिसके अंतर्गत है) नारा बुलंद किया। समाजवादी यथार्थवाद साहित्य के एक विशिष्ट दृष्टिकोण और उसकी एक विशिष्ट शैली का द्योतन करता है अर्थात वह साहित्य या कला की वस्तु और रूप योजना दोनों को घेर लेता है। इसके अतिरिक्त उसमें प्राचीन साहित्य की सजीव परम्पराओं को ग्रहण करने, नई परिस्थितियों के अनुकूल उसका विकास करने एवं कला एवं साहित्य को एक ऐसा मार्ग देने की संभावनाएं मौजूद हैं जिसकी अगली मंजिलें भविष्य के गर्भ में हैं। किन्तु अब तक ‘साहित्य प्रोपैगैंडा है’ का नारा विस्मृत नहीं हो सका है और आवेश में आकर हमारे लेखक इसे दुहराते जाते हैं यहां तक कि अमेरिका के प्रसिद्ध माक्र्सवादी लेखक जोजेफ फ्रीमेन ने भी ‘संयुक्तराष्ट्र में श्रमजीवी साहित्य’ पुस्तक की भूमिका में एक स्थान पर कुछ ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि ‘कला का, जो वर्ग युद्ध का एक साधन यंत्र है, मजदूर वर्ग को अपने एक हथियार के रूप में विकास करना चाहिए।’ उनका कहना है कि कला ‘अनुभव का विनिमय’ करती है। लेकिन ‘अनुभव’ शब्द के अंदर उसकी पकड़ छिपी है। पूंजीवादी विचारक या आलोचक मजदूर वर्ग के जीवन की अभिव्यंजना को अनुभव के अंतर्गत नहीं मानते। बल्कि किसी स्त्री के उरोजों की उपमाओं से भरे वाक्य चमत्कारों को ही अनुभव मानते हैं। फ्रीमेन के पूरे लेख को पढ़ने से यह धारणा तो निर्मूल हो जाती है कि वे इस नारे के अर्थ में साहित्य को वर्गयुद्ध का हथियार मानते हैं। फ्रीमेन का केवल यह कहना है कि साहित्य का प्रयोग चूंकि पूंजीपति वर्ग अपने स्वार्थों की रक्षा के निमित्त कर रहा है, ऐसी दशा में श्रमजीवी वर्ग को भी उसका उपयोग अपने हितों की रक्षा और संघर्ष के विकास में करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि समूचा साहित्य वर्गयुद्ध का हथियार है अथवा उसे होना चाहिए। तो भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग यदि सावधानी से किया जाए तो अच्छा है। यद्यपि इससे, खेद है, हमारे बहुत से पूंजीवादी आलोचकों की मौके-बेमौके फतवा देने की रोजी छिन जाएगी।
चूंकि योरप के अन्य देशों में वर्गयुद्ध एक सफल क्रांति का रूप धारण न कर पाया अतः वहां साहित्य को वर्गयुद्ध का हथियार घोषित करने की उतनी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई जितनी प्रचार का साधन बनाने की, जिससे मजदूर वर्ग का संगठन किया जा सके, उसके अंदर समाजवाद और क्रांति की चेतना फैलाई जा सके। शायद इसीलिए वहां किसी ने यह नारा ईजाद किया कि साहित्य प्रोपैगैंडा है या होता है। पाठकों ने संभव है अमेरिका के प्रसिद्ध समाजवादी उपन्यासकार अप्टन सिंक्लेयर की पुस्तक डंउउवदंतज पढ़ी हो। आलोचना साहित्य की दृष्टि से पुस्तक निम्नकोटि की है और वह प्रगतिवाद के समीक्षा सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन उसमें प्रारम्भ से लेकर रूस की समाजवादी क्रांति तक के योरप और अमेरिका के सभी महान लेखकों और कलाकारों की कृतियों का मूल्यांकन इस दृष्टिकोण को सामने रखकर ही किया गया है कि वे अपने समय के किसी न किसी वर्ग की भावनाओं का प्रोपैगैंडा करती थीं। अप्टन सिंक्लेयर के अनुसार समस्त साहित्य प्रोपैगैंडा है, सार्वभौम तथा अनिवार्य रूप से, कभी अज्ञात रूप से अन्यथा अधिकतर ज्ञात रूप से। कला जीवन की अभिव्यक्ति है जो कलाकार के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है और उसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करना और उन्हें भाव, विश्वास और कार्य परिवर्तन के लिए प्रेरित करना होता है। महान कला का जन्म तभी होता है जब जीवंत तथा महत्वपूर्ण प्रोपैगैंडा कलात्मक नैपुण्य के साथ किसी कला विशेष के माध्यम द्वारा किया जाता है। सिंक्लेयर का कहना केवल इतना है कि यह दावा करना कि कला में प्रोपैगैंडा को स्थान नहीं है अथवा कला का स्वतंत्रता और न्याय की भावनाओं से कोई संबंध नहीं है, एक प्रवंचना है, एक ऐसा भ्रम है जिसे न्यस्त स्वार्थ वाले वर्गों ने फैला रखा है। इसके विपरीत उनके अनुसार कला में प्रोपैगैंडा ही प्रधान प्रेरणा है। क्योंकि साहित्य और कला की प्रत्येक रचना किसी न किसी भाव, विचार, विश्वास या दृष्टिकोण को व्यक्त करती है, और चूंकि अब तक समाज दो या दो से अधिक परस्पर-विरोधी वर्गों में बंटा रहा है, इस कारण यह भाव, विचार, विश्वास या दृष्टिकोण किसी न किसी वर्ग के अनुकूल या प्रतिकूल अवश्य रहते हैं और जब तक मनुष्य वर्गहीन समाज नहीं बना लेता तब तक कला-साहित्य का प्रधान गुण प्रोपैगैंडा ही रहेगा। यदि सिंक्लेयर की प्रोपैगैंडा की इतनी व्यापक व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो प्रोपैगैंडा को कला और साहित्य का एक हद तक सामान्य गुण कहा जा सकता है, पर केवल एक हद तक ही।
सामान्यतः जो लोग आजकल प्रगतिवादियों पर प्रोपैगैंडा के नाम से दोष मढ़ते हैं, वे प्रोपैगैंडा के इतने ही व्यापक अर्थ समझते हैं यद्यपि उसका जो पहलू प्राचीन साहित्य और पूंजीवादी साहित्य पर लागू होता है उसे मानने को तैयार नहीं होते। इन व्यापक अर्थों में प्रोपैगैंडा शब्द से शायद पुराने लेखक और कलाकार इतना न चिढ़ते, वे शायद इस स्वीकार भी कर लेते।
वीरगाथा काल के कवियों को यह स्वीकार करने में क्या संकोच होता कि वे अपने शासक या नरेश के वैभव और पराक्रम की गाथाएं लिखकर उनका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, और क्या यह प्रोपैगैंडा न हुआ? आल्हा, पृथ्वीराजरासो तथा तत्कालीन काव्यग्रंथों में क्या प्रोपैगैंडा नहीं है? और यह बात भी नहीं है कि चंदबरदाई को निम्नकोटि का कवि समझा जाता हो। इसी प्रकार भक्तिकालीन कवियों ने वैष्णव तथा सूफी मतों का प्रचार किया था। तुलसीदास जी की रामायण में ऐसे कितने स्थल नहीं है जहां उन्होंने पाठकों की राम की भक्ति और उपासना के लिए प्रेरित किया है और राम से विमुख जाने वालों के लिए रौरव नरक की भीषण यातनाओं की तस्वीर खींची है।
तुलसीदासजी के इस वर्णन को प्रोपैगैंडा न मानकर यदि ‘शाश्वत सत्य’ मान लिया जाए तो मुझे भय है कि आजकल के भौतिकवादी युग में रौरव-नरक के बन्दियों की संख्या इतनी बढ़ गई होगी कि यमराज को ब्रिटिश सरकार की तरह ‘डिटेन्शन कैम्प’ खुलवाने पड़ रहे होंगे!
मीरा और सूरदास के पदों में भी प्रचार की मात्रा कम नहीं है। फिर भूषण तो, जिन्हें हमारे आलोचक महाकवि स्वीकार करते हैं, यद्यपि यह विवादास्पद है, अपन रचनाओं में खुलेआम महाराज शिवाजी का प्रोपैगैंडा करते थे। उनकी शिवा-बावन आदि से अन्त तक प्रोपैगैंडा प्रधान है। इसी प्रकार आधुनिक लेखकों की रचनाओं में किसी वर्ग या सम्प्रदाय का प्रोपैगैंडा साबित किया जा सकता है। प्रेमचन्द, शरतचन्द्र, टैगोर और इकबाल की कृतियों में भी, जो इस युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हुए हैं, प्रोपैगैंडा की कमी न मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दृष्टिकोण से देखने से कला और साहित्य-कृतियों में प्रोपैगैंडा दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है। पुराने जमाने में लेखक इसे स्वीकार करने से कभी इन्कार न करते, क्योंकि वे इस बात से इन्कार न कर सकते थे कि साहित्य और समाज में अविच्छिन्न संबंध है या कि साहित्य समाज का एक अंग है और वह जीवन की अभिव्यंजना करता है – यद्यपि साहित्य के उपयोग और उद्देश्य के बारे में किसी सामाजिक दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्य आंकने की भाषा से वे अवगत न थे। किन्तु आज के लेखक अक्सर इसे स्वीकार नहीं करते। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि कलाकार समाज की क्रियाशीलता से इतना दूर हो गया है कि उसके मस्तिष्क में ‘कला कला के लिए’ की भ्रामक पूंजीवादी धारणा ने स्थान जमा लिया है। दूसरा यह कि आज वर्ग-संघर्ष इतना तीव्र हो गया है कि इसे स्वीकार करने का अर्थ है कि या जो लेखक यह मान ले कि वह पूंजीपति वर्ग का प्रोपैगैंडा करता है, जो कि एक श्रेष्ठ लेखक कभी कहना मंजूर न करेगा क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उसका भी शोषण कर रखा है, या फिर वह यह स्वीकार कर ले कि वह श्रमजीवी वर्ग का प्रोपैगैंडा करता है, जो कि कहना उसके लिए अनेक कष्टों और यातनाओं और अभिजात वर्ग की उपेक्षा और निन्दा का कारण हो सकता है। अतः आज लेखक ‘संघर्ष से परे रहने’ या तटस्थ रहने का उपक्रम करता है यद्यपि वह ऐसा कर नहीं पाता। विगत युगों के लेखक इस प्रकार दो परस्पर-विरोधी अवस्थाओं से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व से बचे रहते थे। उन युगों में वर्गों का संघर्ष अपने ऐतिहासिक विकास की उस प्रारम्भिक अथवा मध्य अवस्था में था जब लेखक या कलाकार के सामने दो में से एक वर्ग का दामन पकड़ना अनिवार्य न हो गया था। अतः प्र्र्र्रगतिवादियों ने यदि कभी साहित्य को प्रोपैगैंडा माना है तो इसी अर्थ में, किसी दूसरे अर्थ में नहीं। यहां यह बात विचारणीय है कि हमारे ये कतिपय आलोचक चन्दबरदायी या भूषण की कविता में अथवा अपनी रचनाओं में व्यक्त उद्गारों में किसी वर्ग का प्रोपैगैंडा नहीं देखते। यदि कोई राजकुमारों और राजकुमारियों, कोमलांगियों और सूटबूटधारी पुरुषों के विषय में लिखता है तो वह उनकी दृष्टि में प्रोपैगैंडा नहीं है किन्तु यदि कोई किसान मजदूर या मुफलिसों की बस्तियों के बारे में लिखता है तो वह प्रोपैगैंडा है। अतः यदि कुछ आलोचक प्रगतिवादियों पर यह आरोप लगाते हैं कि वे समीक्षा सिद्धांतों को तिलांजलि देकर प्राचीन-साहित्य अथवा आधुनिक-साहित्य के अन्दर शासक वर्गों की भावनाओं की अभिव्यक्ति ढूंढ़कर उसे प्रोपैगैंडा कहते हैं तो प्रगतिवादी भी न्यायपूर्वक उनपर आरोप लगा सकते हैं कि वे प्रगतिवादी साहित्य को प्रोपैगैंडा कहते हैं। और खेद इस बात का है कि साहित्य-समीक्षा की प्रणाली की अवहेलना पर रोष प्रकट करने वाले ये आलोचक ही उस प्रणाली को तिरस्कार करने का सबसे पहला अपराध करते हैं। प्रगतिवादी यदि पूंजीवादी वर्ग के प्रोपैगैंडा का आरोप करते हैं तो आलोचक मजदूर वर्ग के प्रोपैगैंडा का। प्रगतिवादियों में कम से कम इतनी ईमानदारी तो अवश्य है कि समस्त साहित्य को प्रोपैगैंडा करकर वे समस्त साहित्य की राशि में शामिल अपने साहित्य को भी प्रोपैगैंडा स्वीकार करते हैं, तथा प्रोपैगैंडा को अपने में एक बुरी चीज नहीं मानते, यदि बुरा मानते हैं तो केवल शोषक वर्गों के प्रोपैगैंडा को, क्योंकि वह शोषण के कायम रखने का साधन बनता है। इसके विपरीत प्रगतिवादियों के विरोधी प्रोपैगैंडा को हेय मानते हैं, लेकिन पूंजीपति वर्ग की भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोपैगैंडा नहीं मानते; उन्हें मनुष्य की शाश्वत भावनाएं मानते हैं, और मजदूर वर्ग की भावनाओं को प्रोपैगैंडा कहते हैं अर्थात उसे हेय समझते हैं। लेकिन यह तो एक विवाद की बात हुई। वास्तव में क्या सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है? यदि सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है तो निश्चय ही पूंजीपति वर्ग की अपेक्षा मजदूर वर्ग का प्रोपैगैंडा ज्यादा अच्छा है।
अमेरिका के एक दूसरे प्रसिद्ध आलोचक-उपन्यासकार जेम्स.टी.फेरेल ने, जो समाजवादी हैं, अपनी पुस्तक । छवजम वद स्पजमतंतल ब्तपजपबपेउ में इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि हमें सबसे पहले प्रोपैगैंडा शब्द की व्याख्या निश्चित कर लेनी चाहिए। लेनिन की पुस्तक ॅींज प्े ज्व ठम क्वदमघ् से एक उद्धरण देकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि प्रोपैगैंडा किन्हीं सिद्धांतों, योजनाओं तथा विचारों का प्रचार होता है ताकि किसी प्रोगैम या कार्यक्रम के अनुसार शीघ्र ही अमल किया जा सके। फेरेल का कथन है कि यदि इस व्याख्या को स्वीकार किया जाय तो साहित्य को प्रोपैगैंडा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माक्र्स का ‘कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो’ प्रोपैगैंडा की चीज होकर भी न केवल विचार-परिपाक का सुन्दर नमूना है, बल्कि एक श्रेष्ठ साहित्यिक रचना भी है; इसके विपरीत आन्द्रे मालरो का उपन्यास डंदश्े थ्ंजम यद्यपि एक उत्कृष्ट रचना है तथापि प्रोपैगैंडा की दृष्टि से उसके विचार विवादास्पद हैं। अतः साहित्य और प्रोपैगैंडा दो भिन्न चीज है, यद्यपि दोनों का किसी भी रचना में सम्मिश्रण भी होता रहता है। फेरेल ने इससे यह सिद्ध किया है कि साहित्य के अपने अलग नियम होते हैं जिनसे उसको उत्कृष्टता का अन्दाजा लगाया जाता है। साहित्य में केवल सामयिक तत्व ही नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो उसे सापेक्ष्य स्थायित्व का गुण प्रदान करते हैं। अतः फेरेल की राय है कि ‘सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है’ इस नारे को त्याग देना चाहिए और उसके स्थान पर ‘साहित्य सामाजिक प्रभाव का अस्त्र है’ रखना चाहिए।
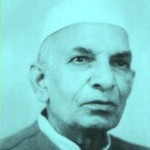
जेम्स टी.फेरेल से मैं कहां तक सहमत हूं, यह ज्यादा महत्व की बात नहीं है, यद्यपि यह स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं फेरेल द्वारा की गई प्रोपैगैंडा की व्याख्या से सहमत हूं। महत्व की बात यह प्रश्न है कि साहित्य की ऐसी समाज-शास्त्रीय व्याख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये व्याख्याएं चाहे जितनी सर्वमान्य क्यों न हों, कहां तक साहित्य की परिभाषा के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं, अर्थात कहां तक वे हमें साहित्य का मूल्यांकन करने में सहायता देती हैं, अतः हमारे समीक्षा-शास्त्र के अन्तर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं। श्री सुमित्रानन्दन पंत की ‘पल्लव’ की भूमिका का यह वाक्य कि ‘हम ब्रज की जीर्ण-शीर्ण छिद्रों से भरी पुरानी छीट की चोली नहीं चाहते, इसकी संकीर्ण कारा में बन्द हो हमारी आत्मा वायु की न्यूनता के कारण सिसक उठती है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है’ विचारणीय है। इस वाक्य की शैली चाहे कितनी ही अलंकृत और पुरानी क्यों न लगे – या अनुपयुक्त भी कह सकते हैं – लेकिन यह समीक्षा प्रणाली के एक नए विकास की ओर अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश करता है। पहले जब सामंती काल में कविता मनोरंजन या आनन्द प्रदान करने के लिए लिखी जाती थी, तब कविता का ‘उद्देश्य’ रस का उद्रेक करना था। और समाज का संगठन ऐसा था कि कविता या साहित्य के ‘उपयोग’ का कभी प्रश्न ही नहीं उठता था। ‘उद्देश्य’ के अन्दर ही ‘उपयोग’ शामिल था, अर्थात दोनों को एक ही मान लिया गया था। और इस ‘उद्देश्य’ या उसमें शामिल ‘उपयोग’ की सीमाएं बहुत संकीर्ण थीं। इस कारण इस ‘उद्देश्य’ की प्राप्ति के लिए इसी सीमित परिधि के अन्दर प्रयोग किये जाते थे और इन प्रयोगों को सफल बनाने के प्रधान अस्त्र थे: अलंकार, ध्वनि, शब्द शक्तियां, वक्रोक्ति, गुण आदि। जहां तक समाजशास्त्र, दर्शन या मनोविज्ञान का संबंध था, उनके अपने अलग बाड़े थे, और यह आवश्यक न समझा जाता था कि इन सब बाड़ों में यातायात की आवश्यकता है। यह रीतिकाल की बात है। उसके पहले भी भक्तिकाल में जब काव्य की आत्मा के स्थान पर धर्म और नैतिकता विराजमान थे आलोचना-पद्धति किसी सामाजिक दृष्टिकोण का अवलम्ब लेकर काव्य का मूल्यांकन नहीं करती थी। छन्दशास्त्र और अलंकारशास्त्र, ये ही इस काव्य-समीक्षा रथ के दो पहिये थे; और रसवाद का सिद्धांत उसके लक्ष्य या उद्देश्य की ओर एक अस्पष्ट इशारा मात्र करता था। भाव या रूप के ‘सौंदर्य’ का कुछ नियमों के अनुसार निरूपण करना ही शास्त्रीय समीक्षा का उद्देश्य था। काल-स्थित समाज में काव्य या साहित्य का क्या उपयोग है, और उसके अनुकूल उसका क्या उद्देश्य है, अर्थात उसका संविधायक पहलू क्या है, इस ओर किसी का ध्यान न जाता था मानो ये प्रश्न साहित्य या कला के मूल्यांकन में असंगत हों, और न कविता या साहित्य की सृष्टि के मानसिक उद्गम तक पहुंचने की कोशिश होती थी, अर्थात मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता न समझी जाती थी – सत्य तो यह है कि यह शास्त्र उस समय न हमारे यहां था और न योरप में ही। अतः कुछ मनस्थितियों या मनोविकारों के वर्णन तक ही समीक्षा सीमित थी, जिसमें श्रृंगार या वात्सल्य, वीर या रौद्र, अद्भुत या वीभत्स, करुण या हास्य रसों के, जो मनस्थितियों का अनुपयुक्त द्योतन करते हैं, परिपाक को दिखाकर विश्रांति ले ली जाती थी। इस प्रकार हमारी प्राचीन समीक्षा-प्रणाली का क्षेत्र इतना संकीर्ण था कि समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक-विश्लेषणशास्त्र के विकास के साथ – यद्यपि इन दोनों शास्त्रों का विकास योरप में हुआ – उसकी संकीर्ण सीमाओं का टूटना आवश्यक हो गया, और कविता या साहित्य जो अब तक प्राचीन समीक्षाशास्त्र की श्रृंखलाओं में जकड़ा था, उसको भी नए ज्ञान के साथ अपना सीमा-विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर पंतजी के उद्धरण को देखें तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ब्रज-काव्य-प्रणाली की ‘संकीर्ण कारा में बन्द हो’ ‘वायु की न्यूनता’ से ‘आत्मा का सिसक उठना’ और ‘शरीर का विकास रुक जाना’ इस अनुभूति का द्योतक है कि काव्य और साहित्य का विकास तब तक रुका रहेगा जब उसका सीमा-विस्तार नहीं किया जाता; और यह सीमा विस्तार समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के नए दृष्टिकोण का भी सूचक है, कि समीक्षाशास्त्र को भी ‘छीट की चोली’ का रंग-बिरंगापन ही नहीं देखना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ‘वायु की न्यूनता’ से आत्मा और शरीर का विकास तो नहीं रुकता। इस सांकेतिक शब्दावली को हटा दें तो इसका अर्थ है कि काव्य और साहित्य के उद्देश्य और उपयोग को हमें फिर से जांचना चाहिए और उनके जांचने के लिए हमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के मापदण्डों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह कि समाजशास्त्र के मापदण्डों से मूल्यांकन करने की प्रथा का श्रीगणेश प्रगतिवादियों के पहले ही शुरू हो गया था। साहित्य के संविधायक पहलू से उसपर विचार किया जाने लगा था। और ‘सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है’, साहित्य के इसी संविधायक दृष्टिकोण का एक उत्तर है। लेकिन यहां हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सारे साहित्य को प्रोपैगैंडा या सामाजिक-प्रभाव का अस्त्र कहकर आज के समाज में उसके एक महत्वपूर्ण संविधायक पहलू का ही निर्देश किया जाता है, और केवल इस दृष्टि से खरी उतरनेवाली कोई रचना अपने में श्रेष्ठ नहीं हो जाती। उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते समय उसकी सौंदर्यानुभूति, उसकी रूपयोजना, शैली और प्रौढ़ता, वाक्य-रचना, शब्द-प्रयोग आदि अनेक दूसरी कसौटियों पर भी उसे कसना आवश्यक है, और प्रगतिवादी इन सब कसौटियों पर भी काव्य या साहित्य-कृति का कसना आवश्यक समझते हैं, उनके महत्व को जानते हैं, यद्यपि आज के संक्रमण-काल में वे साहित्य के संविधायक पहलू को दृष्टि में रखकर उसका सामाजिक दृष्टिकोण से विवेचन करना अधिक आवश्यक समझते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला तो यह कि आज के समाज में कला साहित्य का उपयोग अनेक राजनीतिक और आर्थिक हितों को दृष्टि में रखकर किया जा रहा है, और जो समाज-व्यवस्था को बदलने में संलग्न शक्तियां हैं वे कला-साहित्य के प्रभाव को समझकर भी उन्हें विश्वव्यापी संघर्ष में प्रगतिशील शक्तियों के शक्ति-वर्धन का साधन न बनाए यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण न होगा – यह भाव कला या साहित्य के प्रति अवज्ञा या उपेक्षा का सूचक नहीं है वरन उनके महत्व और उनकी शक्ति के प्रति स्वीकृति का द्योतक है; न यह भाव इस बात का सूचक है कि प्रगतिवादी कला और साहित्य के सौंदर्यगत मूल्य की कद्र नहीं समझते; और न इसका अर्थ है कि प्रगतिवादी साहित्य के संविधायक पहलू पर जोर देकर लेखकों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि कलात्मक दृष्टि से उनकी रचनाएं चाहे कुछ न हो लेकिन आज की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर उनके वक्तव्य चैकस होने चाहिए। दूसरा यह कि प्रगतिवादी यह जानते हैं कि केवल रचना कौशल के कारण ही, और वाक्य-विन्यास या शैली और कला के कारण ही कोई रचना श्रेष्ठ नहीं बन सकती, न पहले कभी बनी – चाहे तब समीक्षक इस पहलू से अवगत न हों, या उसे आवश्यक न समझते हों – न आज बन सकती है, और उसका मूल्यांकन करने के लिए उसके सामाजिक दृष्टिकोण को जांचना भी आवश्यक है, अर्थात कला या साहित्य को सामाजिक उद्देश्य और उपयोग से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों उसके आवश्यक अंग हैं। प्रगतिवादियों पर यदि किसी बात का न्यायोचित आरोप किया जा सकता है तो केवल इस बात का कि वे कला और साहित्य के सामाजिक दृष्टिकोण अर्थात उसके उद्देश्य और उपयोग को ठीक-ठीक स्पष्ट रूप से आंक लेना चाहते हैं और कोरी वायवी, या काल्पनिक, या आदर्शवादी, भावुकता-प्रधान स्थापनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। साहित्य को इतने विस्तृत चैखटे के अन्दर रखकर देखने का प्रयत्न तो अभी शुरू हुआ है, अतः प्रगतिवादी इस नए दृष्टिकोण को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने की ओर प्रयत्नशील हैं, अभी या कभी वे अंतिम निर्णय पर पहुंच जायेंगे, ऐसा कोई भ्रम उन्हें नहीं है। लेकिन सत्य को अधिकाधिक प्राप्त करने का एकमात्र यही तो तरीका है कि हम नित नए अनुभव से अपनी स्थापनाओं को समृद्ध बनाते जांय।
इन विचारों की दृष्टि में यदि हम पुनः ‘क्या साहित्य प्रोपैगैंडा है?’ प्रश्न को जांचें तो हमें उसपर नई रोशनी पड़ती दिखाई देगी। ‘सारा साहित्य प्रोपैगैंडा है’ की स्थापना को अब हम आसानी से अस्वीकृत कर सकते हैं। क्योंकि इस स्थापना में प्रोपैगैंडा की व्याख्या के अनुसार प्रोपैगैंडा और प्रतिपादन को पर्याय मान लिया गया है। लेकिन योजना पर अमल करने या अमल कराने के लिये जनसमूह या उसके किसी अंग को प्रेरित करना एक चीज है और व्यक्ति या समूह के विचारों या भावनाओं का प्रतिपादन करना एक दूसरी चीज है। पहला प्रोपैगैंडा है, दूसरा प्रोपैगैंडा नहीं है। यदि साहित्य में अनिवार्यतः विचारों या भावनाओं का प्रतिपादन मिलता है तो उसे प्रोपैगैंडा नहीं कहा जा सकता। यह दूसरी बात है कि सामाजिक क्रियाशीलता की अभिव्यंजना का साहित्य पाठक को भी उसकी अनुभूति कराता है पर इससे वह प्रोपैगैंडा का पर्याय नहीं बन जाता। लेकिन फेरेल की यह स्थापना उपयुक्त नहीं है कि ‘साहित्य सामाजिक प्रभाव का अस्त्र है।’ यह एक स्वयं सिद्धि है उस तरह की कि आदमी बुद्धि-धारी जानवर है, और अस्त्र जोड़ देने से वह स्वयं सिद्धि न तीव्र हो जाती है न प्रभावपूर्ण। उसके स्थान पर ‘साधन’ ‘चीज’ आदि भी उपयुक्त रहते। इसके अतिरिक्त ‘सामाजिक प्रभाव’ बड़ा कमजोर वाक्यांश है, क्योंकि ‘प्रभाव’ शब्द को सीधे तौर पर सामाजिक प्रगति की अपेक्षा में मापना कठिन है और इस सामाजिक प्रगति में इस प्रभाव की क्या सक्रिय भूमिका रहती है इसका बहुत क्षीण आभास इस शब्द से मिलता है। जिस क्रांतिकारी युग में हम रहते हैं, उसकी वास्तविकता के मुकाबले में यह अभिव्यक्ति अत्यंत लचर है। फिर साहित्य केवल सामाजिक प्रभाव का अस्त्र नहीं है, वह सामाजिक परिवर्तन का भी अस्त्र है। सामाजिक परिवर्तन में साहित्य वह भाव-प्रधान सामाजिक शक्ति उत्पन्न करता है जो मनुष्य के भाव-जगत को परिवर्तित कर इतना विस्तृत बना देती है कि वह हमारे अंदर देखने और अनुभव करने की क्षमता पैदा कर हमें विगत तथा पुरातन के विकसित परिवर्तित रूप आगत तथा नवीन को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है। भाव-जगत का यह परिवर्तन भौतिक जीवन की आवश्यकताओं से प्रभावित होता है और पुनः वह भौतिक जीवन को बदलकर एक उच्च धरातलपर संगठित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह भाव-जगत की क्रिया-प्रक्रिया मनुष्य की स्वतंत्रता प्राप्त करने की जीवन-क्रिया का एक अनिवार्य अंग है। श्रेष्ठ साहित्य इस क्रिया में सहायक होता है, सहायक ही नहीं उसका साधन भी बनता है। श्रेष्ठ कला या साहित्य का यह गुण है। अतः यदि हमें साहित्य की कोई संविधायक स्थापना करनी ही है और यह कहना मुश्किल है कि आज की संघषपूर्ण परिस्थिति में उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, तो हमें स्वर्गीय काॅडवेल की स्थापना स्वीकार करनी चाहिए कि ‘साहित्य या कला मनुष्य की स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक साधन है।’ इसमें ‘स्वतंत्रता’ शब्द विवादास्पद है अवश्य, और उसका उत्तर विज्ञान और दर्शन देने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उसमें अन्य स्थापनाओं के दोष नहीं हैं, और उत्कृष्ट कला या साहित्य के प्रति तो असीम श्रद्धा का भाव है।